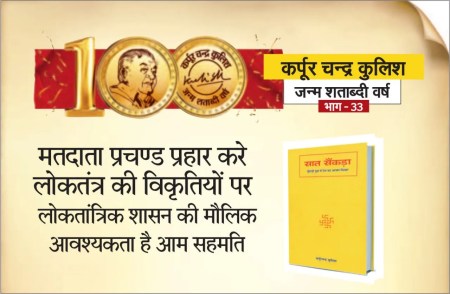
भारतीय लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसकी जड़ें पाताल से भी गहरी है। इन जड़ों को गहरी करने में सबसे अहम योगदान रहा है इस देश के मतदाता का जो हर चुनावों के मौकों पर किसी धारा के बहाव में आने के बजाय नीर-क्षीर विवेक में विश्वास करता है। सत्तर व अस्सी के दशक के चुनावों में मतदान के पूर्व और चुनाव नतीजे आने के बाद कुलिश जी ने मतदाता की ताकत का जिक्र अपने आलेखों में किया। बिहार विधानसभा व राज्यों में उपचुनावों के संदर्भ में प्रासंगिक उनके आलेखों के प्रमुख अंश:
देश के सामने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को निखारना। पिछले एक दशक से हमारी शासन व्यवस्था में जो विकृति बढ़ती देखी जा रही है, वह यह है कि शासन अपने दैनिक कार्यकलाप में आम सहमति के बजाय पुलिस और फौज पर निर्भर करता आ रहा है और देश के राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। परिपाटियां और संस्थाएं छिन्न-भिन्न होती जा रही है। असहमति को सहन नहीं किया जा रहा बल्कि असहमति को पशुबल, प्रलोभन या छल-छद्म से दबाया जा रहा है। व्यक्तिपूजा का भाव बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक शासन की मौलिक आवश्यकता है आम सहमति, विचार विमर्श, स्वस्थ परिपाटियां और साधनों की स्वच्छता। ये उदात्तता तिरोहित होती जा रही है। मतदाता के सामने आज उपयुक्त अवसर है कि वह इन पहलुओं पर विचार करे। उसका प्रचण्ड प्रहार उन विकृतियों पर होना चाहिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में घर कर गई है। नेतृत्व के लिए सुदृढ़- सुचारु व्यवस्था सर्वोपरि है। यदि कोई एक व्यक्ति नेतृत्व के लिए उपयुक्त या उपलब्ध नहीं है, तो संयुक्त नेतृत्व की स्थापना की जा सकती है। मिलीजुली सरकार की स्थापना को न तो सैद्धांतिक आधार पर और न ही व्यावहारिक आधार पर नकारा जाना चाहिए। यह देश तो वैसे ही विविधताओं से भरा हुआ है। यही नहीं बल्कि विविधता इस देश की एक विशेषता है। इस देश में एक ही नेतृत्व परम्परा का पक्ष लेना कदापि उचित नहीं होगा बल्कि परिवर्तन का क्रम चलाना ही होगा।
यह देखा जा रहा, सबसे कम बुराइयां किसमें
एक तरह से यह दौर अच्छा है कि चुनाव में किसी लहर या भावुकता का दौर नहीं है। अत्यधिक भावुकता में सोच विचार या विवेक को अवसर नहीं मिलता। उम्मीदवार, मतदाताओं पर हावी रहता है। राजनीतिक दल मतदाता को उचित सम्मान नहीं देते। बढ़चढ़ कर बातें करते हैं। भावुकता में मतदाता का प्रभाव कम हो जाता है। एक प्रवाह में आम लोग बह जाते हैं और बाद में हाथ मलते दिखाई देते हैं। चुनाव प्रचार में किसी तरह की लहर न हो तो मतदाता को सोच-विचार का अवसर भी मिला है। वह प्रत्येक दल के उम्मीदवारों, कार्यक्रमों और पिछले अनुभवों की तुलनात्मक समीक्षा करता है। इन तुलनाओं में कार्यक्रम और विचारधारा का पक्ष अब प्राय: गौण हो गया है तथा उम्मीदवार और संबंधित दल का आचरण प्रधान विषय बन गया है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों में अच्छाइयां खोजना अब जनसाधारण ने बंद कर दिया है। बल्कि यह देखा जा रहा है कि सबसे कम बुराइयां किस में हैं। राजनीति अब अनचाही चीज या मजबूरी बन गई हे। राजनेेताओं के आचरण के प्रति भी और राजनीतिक दलों की कार्यशैली के कारण मतदाताओं में इतनी ग्लानि भर गई है कि वे सहज ही किसी को विश्वास देने को तैयार नहीं है। इन चुनावों में आम जनता यह भी सोचती है कि यदि किसी को वोट दिया भी तो क्या पता वह उस दल में रहेगा भी या नहीं जिसके निशान पर चुनाव लड़ रहा है।
(31 दिसम्बर 1979 के अंक में ‘हर उम्मीदवार कठघरे में’ शीर्षक आलेख से )
लोकतंत्र में गहरी आस्था
पिछले दो चुनावों की भांति ही इन चुनावों में भी परिणामों के बारे में सारे अनुमान विफल हो गए और आकलन का कोई मापदण्ड काम नहीं आया। अलबत्ता यह निरंतरता देखने में आई कि लोकतंत्र में भारतीय मतदाता की गहरी आस्था है। चुनाव का आह्वान होते ही वह अपना मन बनाकर मतदान केन्द्र तक पहुंच जाता है। इसी तरह सात चुनाव शांतिपूर्वक हो चुके हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश को मतदाता की इस परिपक्वता पर गर्व होगा। उसके फैसले को नतमस्तक हो स्वीकार करना होगा। राजनीतिक दलों को नए सिरे से देश की समस्याओं के समाधान में अपने-अपने तरीके से योगदान करना होगा। जरूरी है राजनीतिक दल स्वस्थ राष्ट्रीय सहमति का दृष्टिकोण अपनाएं।
(8 जनवरी 1980 को ‘1980 का फैसला’ शीर्षक अग्रलेख से)
Published on:
06 Nov 2025 08:37 pm

